जिलाधिकारी ने थाना धानेपुर में जनसमस्याओं की सुनवाई कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु अधिकारियों को दिये निर्देश

*गोण्डा 28 फरवरी,2026*।
प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान के उद्देश्य से थाना धानेपुर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा उपस्थित फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
थाना परिसर में आयोजित समाधान दिवस में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से आए नागरिकों ने भूमि विवाद, अवैध कब्जा, रास्ता अवरोध, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि, पारिवारिक विवाद तथा अन्य स्थानीय समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राप्त सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनके निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
उन्होंने कहा कि राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करे तथा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता एवं विपक्षी पक्ष—दोनों को बुलाकर पारदर्शी तरीके से प्रकरण का समाधान कराया जाए, जिससे भविष्य में विवाद की पुनरावृत्ति न हो।
समाधान दिवस के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों के लिए संबंधित विभागों को निश्चित समयसीमा निर्धारित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि आमजन को न्याय पाने के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। समाधान दिवस जैसी पहल जनता और प्रशासन के बीच विश्वास को मजबूत करती है।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें तथा प्रत्येक शिकायत का संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें।
कार्यक्रम में नायब तहसीलदार अनुराग पाण्डेय, थाना प्रभारी तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी ने 147 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास
*सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 40 विकास परियोजनाओं की सौगात
हल्द्वानी। पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में जनपद के लिए कुल 147 करोड़ 28 लाख 56 हजार रुपये की लागत वाली 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
*23 योजनाओं का लोकार्पण, 17 का शिलान्यास
कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज से जुड़ी 23 योजनाओं का लगभग 72 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से लोकार्पण किया गया, जबकि 17 योजनाओं का 74 करोड़ 90 लाख 56 हजार रुपये की लागत से शिलान्यास हुआ।
इन योजनाओं में प्रमुख रूप से —
* शिप्रा नदी पर 30 मीटर स्पान का मोटर पुल निर्माण
* आईटीआई हल्द्वानी में टेक्नोलॉजी लैब स्थापना
* कोटाबाग, महादेवपुरम, झलुवाझाला, बेलपोखरा व बैलपड़ाव में नलकूप निर्माण
* महिला महाविद्यालय में लैब निर्माण
* जल जीवन मिशन के तहत 14 पेयजल योजनाएं
* रामगढ़ में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण
* सड़क और सीवरेज परियोजनाओं को भी मिली रफ्तार
सीएम ने कसियालेख- धारी मोटर मार्ग, रानीबाग-खुटानी सड़क, चाफी- पदमपुरी-धानाचूली मार्ग, 28 एमएलडी एसटीपी निर्माण, नवाबी रोड सीवरेज कार्य और नारीमन तिराहे से गौलापार तक सड़क मरम्मत कार्यों का भी शुभारंभ किया। साथ ही हल्द्वानी काठगोदाम स्रोत एवं ट्रीटमेंट संवर्धन पेयजल योजना (लागत 154 करोड़ 43 लाख रुपये) का भूमि पूजन भी किया गया।
*एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया और नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया।
*वनभूलपुरा प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का आभार
मुख्यमंत्री ने वनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब अंतरिम आदेश के बाद जिला प्रशासन आगे की कार्यवाही करेगा।
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से नैनीताल जनपद में विकास को नई गति मिलेगी और उत्तराखंड विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए सरकार की “विकास और विरासत साथ-साथ” नीति को दोहराया।
कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
दशमेश पब्लिक स्कूल के परिसर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया होली।
मोनू भाटी।
मेरठ जिले में रामराज स्थित दशमेश पब्लिक स्कूल के परिसर में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया । स्कूल के इस प्रांगण में आयोजित इस उत्सव में न केवल छात्र-छात्राओं ने बढ़-कर कर भाग लिया बल्कि शिक्षकों ने भी होली के गीतों पर थिरक कर माहौल को और अधिक खुशनुमा बना दिया ।
इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की डायरेक्टर डॉक्टर सिम्मी सहोता व प्रधानाचार्य आमिर खान ने दीप प्रज्वलन कर किया इसके बाद छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम के महत्व को दर्शाया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा, कान्हा संग ,होली नृत्य पेश कर सबका मनमोह लिया। सभी बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल एवं तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी l
इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा। विद्यालय की डायरेक्टर डॉक्टर सिम्मी सहोता ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए और रासायनिक रंग के स्थान पर हर्बल रंगों को ही प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों स्टाफ सदस्यों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी l
प्रधानाचार्य आमिर खान ने भी सभी को होली की शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि यह त्यौहार समाज में प्रेम और सद्भावना के रंग बिखेरेने का त्यौहार है।
इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर स्वाति अरोड़ा, मनजोत कौर ,हर्षिका अरोड़ा ,गुरजीत कौर ,अमृतपाल कौर ,स्वाति, प्रियंका, मोनिका,कोमल, खुशबू ,हरप्रीत कौर ,प्रभजोत कौर रेनू ,लक्ष्मी, आदि समस्त स्टाफ उपस्थित रहा l

उत्तराखंड में एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत

*155 सरकारी केंद्रों पर 14 वर्षीय किशोरियों को मुफ्त वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर से बचाव की पहल
देहरादून। राज्य में महिला स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तराखंड में एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। देहरादून स्थित गांधी शताब्दी चिकित्सालय से गुरमीत सिंह ने प्रदेशव्यापी अभियान की औपचारिक शुरुआत की।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह पहल सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम और किशोरियों के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में दूरदर्शी कदम है। उन्होंने नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “बेटियां राष्ट्र का भविष्य हैं और स्वस्थ नारी ही परिवार व समाज की सशक्त रीढ़ होती है।”
राज्यपाल ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
अभियान की मुख्य विशेषताएं:
* पहले चरण में प्रदेश के 155 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चिन्हित।
* 14 वर्ष की पात्र किशोरियों को टीका लगाया जाएगा।
* क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी वैक्सीन गार्डासिल का उपयोग, जो वायरस के चार प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करती है।
* निजी क्षेत्र में प्रति डोज कीमत लगभग 4,000 रुपये, जबकि सरकारी संस्थानों में पूरी तरह निशुल्क।
* डॉक्टरों, नर्सों और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण पूर्ण, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध।
- कैंसर रोकथाम की दिशा में बड़ा कदम
एचपीवी टीका सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा), गले के कैंसर और जननांग मस्सों से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है। विशेषज्ञों के अनुसार 9 से 14 वर्ष की आयु में यह टीका सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यह संक्रमण से पहले सुरक्षा देता है।
राज्य सरकार ने इस अभियान को महिला स्वास्थ्य सुधार और कैंसर रोकथाम की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया है, जिससे हजारों किशोरियों को भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकेगा।
यूपी: होली पर हवाई सफर ‘आसमान’ पर: मुंबई-लखनऊ किराया तीन गुना, दिल्ली रूट भी 8 हजार पार
लखनऊ। होली से पहले घर लौटने की तैयारी कर रहे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के बीच हवाई किराए भी अचानक उछाल पर हैं। आम दिनों में करीब 5 हजार रुपये में मिलने वाला मुंबई-लखनऊ का टिकट अब तीन गुना तक पहुंच गया है।
2 मार्च को IndiGo की मुंबई-लखनऊ फ्लाइट का किराया 10,416 रुपये दर्ज किया गया, जबकि Air India की इसी रूट की उड़ान होली वीक में 13,058 रुपये तक बिकी। Akasa Air की फ्लाइट का किराया भी 11,791 रुपये तक पहुंच गया। 3 मार्च को तो कुछ उड़ानों के टिकट 16,193 रुपये तक बिके, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।
दिल्ली-लखनऊ रूट पर भी स्थिति अलग नहीं है। होली से ठीक पहले 3 मार्च को कुछ उड़ानों का किराया 11,893 रुपये तक पहुंच गया, जबकि सामान्य दिनों में यही टिकट 3 से 5 हजार रुपये के बीच उपलब्ध रहता है। कई उड़ानों का किराया 8 हजार रुपये के पार चला गया है।
उधर, रेल यात्रियों की परेशानी भी कम नहीं है। प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है, जिससे बड़ी संख्या में लोग वैकल्पिक साधन तलाशने को मजबूर हैं।
त्योहार के मद्देनजर बढ़ती मांग के कारण हवाई किराए में आई तेज वृद्धि ने आम यात्रियों की जेब पर असर डाला है। ऐसे में होली पर घर लौटना इस बार कई लोगों के लिए चुनौती बन गया है—न ट्रेन में सीट मिल रही है, न फ्लाइट के सस्ते टिकट।
यूपी: होली पर हवाई सफर ‘आसमान’ पर: मुंबई-लखनऊ किराया तीन गुना, दिल्ली रूट भी 8 हजार पार
लखनऊ। होली से पहले घर लौटने की तैयारी कर रहे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के बीच हवाई किराए भी अचानक उछाल पर हैं। आम दिनों में करीब 5 हजार रुपये में मिलने वाला मुंबई-लखनऊ का टिकट अब तीन गुना तक पहुंच गया है।
2 मार्च को IndiGo की मुंबई-लखनऊ फ्लाइट का किराया 10,416 रुपये दर्ज किया गया, जबकि Air India की इसी रूट की उड़ान होली वीक में 13,058 रुपये तक बिकी। Akasa Air की फ्लाइट का किराया भी 11,791 रुपये तक पहुंच गया। 3 मार्च को तो कुछ उड़ानों के टिकट 16,193 रुपये तक बिके, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।
दिल्ली-लखनऊ रूट पर भी स्थिति अलग नहीं है। होली से ठीक पहले 3 मार्च को कुछ उड़ानों का किराया 11,893 रुपये तक पहुंच गया, जबकि सामान्य दिनों में यही टिकट 3 से 5 हजार रुपये के बीच उपलब्ध रहता है। कई उड़ानों का किराया 8 हजार रुपये के पार चला गया है।
उधर, रेल यात्रियों की परेशानी भी कम नहीं है। प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है, जिससे बड़ी संख्या में लोग वैकल्पिक साधन तलाशने को मजबूर हैं।
त्योहार के मद्देनजर बढ़ती मांग के कारण हवाई किराए में आई तेज वृद्धि ने आम यात्रियों की जेब पर असर डाला है। ऐसे में होली पर घर लौटना इस बार कई लोगों के लिए चुनौती बन गया है—न ट्रेन में सीट मिल रही है, न फ्लाइट के सस्ते टिकट।
डंपर की टक्कर से युवक-युवती की दर्दनाक मौत, आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम
हल्द्वानी, उत्तराखंड। हल्द्वानी-लालकुआं हाईवे पर बेरीपड़ाव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक-युवती की मौत हो गई। तेज रफ्तार डंपर ने दोनों को कुचल दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।
हादसे में 30 वर्षीय कार्तिक कांडपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 वर्षीय नेहा कांडपाल गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उन्होंने भी दम तोड़ दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर तेज गति से आ रहा था और अनियंत्रित होकर स्कूटी को टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।
दुर्घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने डंपर चालकों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है।
साई कॉलेज में विज्ञान दिवस पर आयोजित हुई पोस्टर प्रदर्शनी
अम्बिकापुर- श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर में शनिवार को साईंस क्लब के तत्वावधान में विज्ञान दिवस मनाया गया। कैटलाइजिंग विकसित भारत थ्रू इंडियन नॉलेज सिस्टम इन साईंस विषय पर पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित हुई जिसमें विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा की जरूरत, कृत्रिम बुद्धि की दक्षता, मेक इन इंडिया, आर्थिक शक्ति के रूप में भारत, अंतरिक्ष में भारतीय क्षमता का प्रदर्शन, विज्ञान में प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली को कैनवास पर उकेरा। साईंस क्लब के प्रभारी दीपक तिवारी ने बताया कि विद्याथियों ने पोस्टर पर भारतीय ज्ञान परम्परा के इतिहास और विकास को दर्शाया है तो दूसरी ओर हरित ऊर्जा को 21 सदी की जरूरत बताया। संख्ययों की गणना हमारे मानवीय विकास की आधारशिला है। पोस्टर में संख्याओं के विकास और प्रक्रिया को दर्शाया गया है जो रोमांचक रहा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड हमारी पहचान से जुड़ा है जो हमारी मानवीय विकास की यात्रा है।
एजूकेशन फॉर ऑल, जस्टिस फॉल ऑल के साथ वसुधैव कुटुम्बकम् का उद्घोष नजर आया। प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। प्रदर्शनी के दौरान डॉ. श्रीराम बघेल, विभा तिवारी, कंचन साहू, राहुल कुंडू, नीरज राजवाड़े आदि ने सहयोग किया।
प्रदर्शनी के दौरान आईक्यूएसी प्रभारी डॉ. शैलेष देवांगन, एनईपी प्रभारी डॉ. आर.एन. शर्मा, कम्प्यूटर एंड आईटी विभाग के अध्यक्ष डॉ. विवेक कुमार गुप्ता, लाइफ साईंस विभाग के अध्यक्ष अरविन्द तिवारी, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. दिनेश शाक्य और वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग के अध्यक्ष राकेश कुमार सेन तथा सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
धनबाद निकाय चुनाव परिणाम: पुराने दिग्गजों का तिलिस्म टूटा, मनोरंजन सिंह की जीत की हैट्रिक।

धनबाद नगर निगम चुनाव इस बार कई मायनों में बेहद रोचक रहा. मतदाताओं ने जहां कुछ पुराने चेहरों पर दोबारा भरोसा जताया, वहीं कई दिग्गजों का तिलिस्म टूट गया. शुक्रवार को 55 में से 14 वार्डों के परिणाम घोषित हुए, जबकि शेष 41 वार्डों के नतीजे शनिवार को जारी होने हैं. वार्ड नंबर 28 से मनोरंजन सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए लगातार तीसरी बार पार्षद पद पर कब्जा जमाया. पिछली बार महिला आरक्षण के कारण उनकी पत्नी पूजा कुमारी चुनाव मैदान में उतरी थीं और जीत दर्ज की थी. इस बार चुनाव मैदान में उतरे मनोरंजन सिंह ने जीत दर्ज की. वहीं तीन बार पार्षद रह चुके निर्मल मुखर्जी को इस बार हार का सामना करना पड़ा. विकास रंजन ने उन्हें शिकस्त दी.
अरुणा ने दूसरी बार दर्ज की जीत
अरुणा कुमारी ने दूसरी बार जीत दर्ज कर अपनी सीट बरकरार रखी. हालांकि, वर्ष 2010 में उनके पति अशोक यादव ने इस वार्ड से जीत हासिल की थी. मीनाक्षी सिंह ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर अपना प्रभाव कायम रखा. इस वार्ड में पहले मीनाक्षी सिंह ने दर्ज की थी. दूसरी बार उनकी सास उषा सिंह जीत दर्ज की थी. कार्यकाल में ही उषा सिंह के निधन पर मिड टर्म में चुनाव हुआ था, जिसमें उनकी ननद सुमन सिंह ने जीत दर्ज की थी. इससे यह सीट लंबे समय से एक ही परिवार के कब्जे में रही. इधर, अंदिला कुमारी को मतदाताओं ने इस बार नकार दिया. पूर्व पार्षद प्रफुल्ल मंडल की पत्नी उर्मिला मंडल ने उन्हें हराया. वहीं वार्ड नंबर 52 से पूर्व पार्षद प्रियंका देवी को भी हार का सामना करना पड़ा. लक्ष्मी कुमारी ने उन्हें शिकस्त दी.
कड़ी सुरक्षा में मतगणना
धनबाद नगर निकाय चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पॉलिटेक्निक परिसर में जारी है. पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह की अव्यवस्था या हंगामे की आशंका को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं. पूरे परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं. एसएसपी प्रभात कुमार स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं. उनके नेतृत्व में सिटी एसपी सहित कई थाना प्रभारियों और बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की ड्यूटी लगाई गई है.
कई स्थानों पर की गई बैरिकेडिंग
भीड़ व समर्थकों को मतगणना स्थल से दूर रखने के लिए बेकारबांध स्थित चंद्रशेखर आजाद चौक पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है. वहीं, वीआइपी कॉलोनी मोड़ पर भी बैरिकेडिंग की गई है. दोनों स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी व जवानों की तैनाती की गई है. यहां आने-जाने वाले वाहनों और लोगों की सघन जांच की जा रही है. बिना पास के किसी को भी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है. इसके अलावा, कई थानों में अतिरिक्त पुलिस बल को रिजर्व रखा गया है. काउंटिंग स्थल के अंदर व बाहर दंडाधिकारी भी तैनात हैं.
नौरादेही टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत पर कर्मचारियों पर फटकार, कार्रवाई के आदेश
सागर, मध्यप्रदेश। कान्हा टाइगर रिजर्व से जनवरी में नौरादेही शिफ्ट किए गए बाघ की मौत मामले में कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हुई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख ने नौरादेही डीएफओ रजनीश कुमार सिंह को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि दोषी कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
प्रतिवेदन के अनुसार, बाघ को कान्हा से लाने के बाद 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही थी। 13 फरवरी को बाघ की लोकेशन लगातार एक ही स्थान पर मिलने के बावजूद मॉनिटरिंग टीम मौके पर नहीं पहुंची। जब टीम 48 घंटे बाद पहुंची, तो बाघ मृत पाया गया। पोस्टमार्टम में बाघ की खोपड़ी पर अन्य बाघ के केनाइन दांत के निशान और हड्डियों में टूटने के लक्षण मिले, जिससे पता चलता है कि बाघ टेरिटोरियल फाइट के दौरान मारा गया।
वन मुख्यालय ने कहा कि स्थानीय कर्मचारियों ने बाघ की लड़ाई और घायल होने की स्थिति को अनसुना किया, जबकि निर्देश थे कि इस दौरान घायल बाघ की तुरंत मॉनिटरिंग और आवश्यक उपचार किया जाए।
वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने कहा कि बाघ के लिए महंगा सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाया गया था और पूरी टीम निगरानी में लगी हुई थी। दुर्भाग्य से बाघ दो दिन तक मृत पड़ा रहा, लेकिन क्विक रिस्पांस टीम इसे समय पर नहीं देख पाई। उन्होंने प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख से दोषियों पर सख्त कार्रवाई का अनुरोध किया।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख ने डीएफओ को आदेश दिया है कि लापरवाह कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और भविष्य में रेडियो कॉलरधारी बाघ और अन्य बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वन विभाग का लक्ष्य है कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो और वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे।
जिलाधिकारी ने थाना धानेपुर में जनसमस्याओं की सुनवाई कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु अधिकारियों को दिये निर्देश

*गोण्डा 28 फरवरी,2026*।
प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान के उद्देश्य से थाना धानेपुर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा उपस्थित फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
थाना परिसर में आयोजित समाधान दिवस में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से आए नागरिकों ने भूमि विवाद, अवैध कब्जा, रास्ता अवरोध, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि, पारिवारिक विवाद तथा अन्य स्थानीय समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राप्त सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनके निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
उन्होंने कहा कि राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करे तथा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता एवं विपक्षी पक्ष—दोनों को बुलाकर पारदर्शी तरीके से प्रकरण का समाधान कराया जाए, जिससे भविष्य में विवाद की पुनरावृत्ति न हो।
समाधान दिवस के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों के लिए संबंधित विभागों को निश्चित समयसीमा निर्धारित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि आमजन को न्याय पाने के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। समाधान दिवस जैसी पहल जनता और प्रशासन के बीच विश्वास को मजबूत करती है।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें तथा प्रत्येक शिकायत का संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें।
कार्यक्रम में नायब तहसीलदार अनुराग पाण्डेय, थाना प्रभारी तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी ने 147 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास
*सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 40 विकास परियोजनाओं की सौगात
हल्द्वानी। पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में जनपद के लिए कुल 147 करोड़ 28 लाख 56 हजार रुपये की लागत वाली 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
*23 योजनाओं का लोकार्पण, 17 का शिलान्यास
कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज से जुड़ी 23 योजनाओं का लगभग 72 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से लोकार्पण किया गया, जबकि 17 योजनाओं का 74 करोड़ 90 लाख 56 हजार रुपये की लागत से शिलान्यास हुआ।
इन योजनाओं में प्रमुख रूप से —
* शिप्रा नदी पर 30 मीटर स्पान का मोटर पुल निर्माण
* आईटीआई हल्द्वानी में टेक्नोलॉजी लैब स्थापना
* कोटाबाग, महादेवपुरम, झलुवाझाला, बेलपोखरा व बैलपड़ाव में नलकूप निर्माण
* महिला महाविद्यालय में लैब निर्माण
* जल जीवन मिशन के तहत 14 पेयजल योजनाएं
* रामगढ़ में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण
* सड़क और सीवरेज परियोजनाओं को भी मिली रफ्तार
सीएम ने कसियालेख- धारी मोटर मार्ग, रानीबाग-खुटानी सड़क, चाफी- पदमपुरी-धानाचूली मार्ग, 28 एमएलडी एसटीपी निर्माण, नवाबी रोड सीवरेज कार्य और नारीमन तिराहे से गौलापार तक सड़क मरम्मत कार्यों का भी शुभारंभ किया। साथ ही हल्द्वानी काठगोदाम स्रोत एवं ट्रीटमेंट संवर्धन पेयजल योजना (लागत 154 करोड़ 43 लाख रुपये) का भूमि पूजन भी किया गया।
*एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया और नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया।
*वनभूलपुरा प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का आभार
मुख्यमंत्री ने वनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब अंतरिम आदेश के बाद जिला प्रशासन आगे की कार्यवाही करेगा।
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से नैनीताल जनपद में विकास को नई गति मिलेगी और उत्तराखंड विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए सरकार की “विकास और विरासत साथ-साथ” नीति को दोहराया।
कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
दशमेश पब्लिक स्कूल के परिसर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया होली।
मोनू भाटी।
मेरठ जिले में रामराज स्थित दशमेश पब्लिक स्कूल के परिसर में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया । स्कूल के इस प्रांगण में आयोजित इस उत्सव में न केवल छात्र-छात्राओं ने बढ़-कर कर भाग लिया बल्कि शिक्षकों ने भी होली के गीतों पर थिरक कर माहौल को और अधिक खुशनुमा बना दिया ।
इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की डायरेक्टर डॉक्टर सिम्मी सहोता व प्रधानाचार्य आमिर खान ने दीप प्रज्वलन कर किया इसके बाद छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम के महत्व को दर्शाया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा, कान्हा संग ,होली नृत्य पेश कर सबका मनमोह लिया। सभी बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल एवं तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी l
इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा। विद्यालय की डायरेक्टर डॉक्टर सिम्मी सहोता ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए और रासायनिक रंग के स्थान पर हर्बल रंगों को ही प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों स्टाफ सदस्यों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी l
प्रधानाचार्य आमिर खान ने भी सभी को होली की शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि यह त्यौहार समाज में प्रेम और सद्भावना के रंग बिखेरेने का त्यौहार है।
इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर स्वाति अरोड़ा, मनजोत कौर ,हर्षिका अरोड़ा ,गुरजीत कौर ,अमृतपाल कौर ,स्वाति, प्रियंका, मोनिका,कोमल, खुशबू ,हरप्रीत कौर ,प्रभजोत कौर रेनू ,लक्ष्मी, आदि समस्त स्टाफ उपस्थित रहा l

उत्तराखंड में एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत

*155 सरकारी केंद्रों पर 14 वर्षीय किशोरियों को मुफ्त वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर से बचाव की पहल
देहरादून। राज्य में महिला स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तराखंड में एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। देहरादून स्थित गांधी शताब्दी चिकित्सालय से गुरमीत सिंह ने प्रदेशव्यापी अभियान की औपचारिक शुरुआत की।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह पहल सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम और किशोरियों के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में दूरदर्शी कदम है। उन्होंने नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “बेटियां राष्ट्र का भविष्य हैं और स्वस्थ नारी ही परिवार व समाज की सशक्त रीढ़ होती है।”
राज्यपाल ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
अभियान की मुख्य विशेषताएं:
* पहले चरण में प्रदेश के 155 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चिन्हित।
* 14 वर्ष की पात्र किशोरियों को टीका लगाया जाएगा।
* क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी वैक्सीन गार्डासिल का उपयोग, जो वायरस के चार प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करती है।
* निजी क्षेत्र में प्रति डोज कीमत लगभग 4,000 रुपये, जबकि सरकारी संस्थानों में पूरी तरह निशुल्क।
* डॉक्टरों, नर्सों और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण पूर्ण, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध।
- कैंसर रोकथाम की दिशा में बड़ा कदम
एचपीवी टीका सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा), गले के कैंसर और जननांग मस्सों से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है। विशेषज्ञों के अनुसार 9 से 14 वर्ष की आयु में यह टीका सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यह संक्रमण से पहले सुरक्षा देता है।
राज्य सरकार ने इस अभियान को महिला स्वास्थ्य सुधार और कैंसर रोकथाम की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया है, जिससे हजारों किशोरियों को भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकेगा।
यूपी: होली पर हवाई सफर ‘आसमान’ पर: मुंबई-लखनऊ किराया तीन गुना, दिल्ली रूट भी 8 हजार पार
लखनऊ। होली से पहले घर लौटने की तैयारी कर रहे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के बीच हवाई किराए भी अचानक उछाल पर हैं। आम दिनों में करीब 5 हजार रुपये में मिलने वाला मुंबई-लखनऊ का टिकट अब तीन गुना तक पहुंच गया है।
2 मार्च को IndiGo की मुंबई-लखनऊ फ्लाइट का किराया 10,416 रुपये दर्ज किया गया, जबकि Air India की इसी रूट की उड़ान होली वीक में 13,058 रुपये तक बिकी। Akasa Air की फ्लाइट का किराया भी 11,791 रुपये तक पहुंच गया। 3 मार्च को तो कुछ उड़ानों के टिकट 16,193 रुपये तक बिके, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।
दिल्ली-लखनऊ रूट पर भी स्थिति अलग नहीं है। होली से ठीक पहले 3 मार्च को कुछ उड़ानों का किराया 11,893 रुपये तक पहुंच गया, जबकि सामान्य दिनों में यही टिकट 3 से 5 हजार रुपये के बीच उपलब्ध रहता है। कई उड़ानों का किराया 8 हजार रुपये के पार चला गया है।
उधर, रेल यात्रियों की परेशानी भी कम नहीं है। प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है, जिससे बड़ी संख्या में लोग वैकल्पिक साधन तलाशने को मजबूर हैं।
त्योहार के मद्देनजर बढ़ती मांग के कारण हवाई किराए में आई तेज वृद्धि ने आम यात्रियों की जेब पर असर डाला है। ऐसे में होली पर घर लौटना इस बार कई लोगों के लिए चुनौती बन गया है—न ट्रेन में सीट मिल रही है, न फ्लाइट के सस्ते टिकट।
यूपी: होली पर हवाई सफर ‘आसमान’ पर: मुंबई-लखनऊ किराया तीन गुना, दिल्ली रूट भी 8 हजार पार
लखनऊ। होली से पहले घर लौटने की तैयारी कर रहे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के बीच हवाई किराए भी अचानक उछाल पर हैं। आम दिनों में करीब 5 हजार रुपये में मिलने वाला मुंबई-लखनऊ का टिकट अब तीन गुना तक पहुंच गया है।
2 मार्च को IndiGo की मुंबई-लखनऊ फ्लाइट का किराया 10,416 रुपये दर्ज किया गया, जबकि Air India की इसी रूट की उड़ान होली वीक में 13,058 रुपये तक बिकी। Akasa Air की फ्लाइट का किराया भी 11,791 रुपये तक पहुंच गया। 3 मार्च को तो कुछ उड़ानों के टिकट 16,193 रुपये तक बिके, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।
दिल्ली-लखनऊ रूट पर भी स्थिति अलग नहीं है। होली से ठीक पहले 3 मार्च को कुछ उड़ानों का किराया 11,893 रुपये तक पहुंच गया, जबकि सामान्य दिनों में यही टिकट 3 से 5 हजार रुपये के बीच उपलब्ध रहता है। कई उड़ानों का किराया 8 हजार रुपये के पार चला गया है।
उधर, रेल यात्रियों की परेशानी भी कम नहीं है। प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है, जिससे बड़ी संख्या में लोग वैकल्पिक साधन तलाशने को मजबूर हैं।
त्योहार के मद्देनजर बढ़ती मांग के कारण हवाई किराए में आई तेज वृद्धि ने आम यात्रियों की जेब पर असर डाला है। ऐसे में होली पर घर लौटना इस बार कई लोगों के लिए चुनौती बन गया है—न ट्रेन में सीट मिल रही है, न फ्लाइट के सस्ते टिकट।
डंपर की टक्कर से युवक-युवती की दर्दनाक मौत, आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम
हल्द्वानी, उत्तराखंड। हल्द्वानी-लालकुआं हाईवे पर बेरीपड़ाव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक-युवती की मौत हो गई। तेज रफ्तार डंपर ने दोनों को कुचल दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।
हादसे में 30 वर्षीय कार्तिक कांडपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 वर्षीय नेहा कांडपाल गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उन्होंने भी दम तोड़ दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर तेज गति से आ रहा था और अनियंत्रित होकर स्कूटी को टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।
दुर्घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने डंपर चालकों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है।
साई कॉलेज में विज्ञान दिवस पर आयोजित हुई पोस्टर प्रदर्शनी
अम्बिकापुर- श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर में शनिवार को साईंस क्लब के तत्वावधान में विज्ञान दिवस मनाया गया। कैटलाइजिंग विकसित भारत थ्रू इंडियन नॉलेज सिस्टम इन साईंस विषय पर पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित हुई जिसमें विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा की जरूरत, कृत्रिम बुद्धि की दक्षता, मेक इन इंडिया, आर्थिक शक्ति के रूप में भारत, अंतरिक्ष में भारतीय क्षमता का प्रदर्शन, विज्ञान में प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली को कैनवास पर उकेरा। साईंस क्लब के प्रभारी दीपक तिवारी ने बताया कि विद्याथियों ने पोस्टर पर भारतीय ज्ञान परम्परा के इतिहास और विकास को दर्शाया है तो दूसरी ओर हरित ऊर्जा को 21 सदी की जरूरत बताया। संख्ययों की गणना हमारे मानवीय विकास की आधारशिला है। पोस्टर में संख्याओं के विकास और प्रक्रिया को दर्शाया गया है जो रोमांचक रहा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड हमारी पहचान से जुड़ा है जो हमारी मानवीय विकास की यात्रा है।
एजूकेशन फॉर ऑल, जस्टिस फॉल ऑल के साथ वसुधैव कुटुम्बकम् का उद्घोष नजर आया। प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। प्रदर्शनी के दौरान डॉ. श्रीराम बघेल, विभा तिवारी, कंचन साहू, राहुल कुंडू, नीरज राजवाड़े आदि ने सहयोग किया।
प्रदर्शनी के दौरान आईक्यूएसी प्रभारी डॉ. शैलेष देवांगन, एनईपी प्रभारी डॉ. आर.एन. शर्मा, कम्प्यूटर एंड आईटी विभाग के अध्यक्ष डॉ. विवेक कुमार गुप्ता, लाइफ साईंस विभाग के अध्यक्ष अरविन्द तिवारी, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. दिनेश शाक्य और वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग के अध्यक्ष राकेश कुमार सेन तथा सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
धनबाद निकाय चुनाव परिणाम: पुराने दिग्गजों का तिलिस्म टूटा, मनोरंजन सिंह की जीत की हैट्रिक।

धनबाद नगर निगम चुनाव इस बार कई मायनों में बेहद रोचक रहा. मतदाताओं ने जहां कुछ पुराने चेहरों पर दोबारा भरोसा जताया, वहीं कई दिग्गजों का तिलिस्म टूट गया. शुक्रवार को 55 में से 14 वार्डों के परिणाम घोषित हुए, जबकि शेष 41 वार्डों के नतीजे शनिवार को जारी होने हैं. वार्ड नंबर 28 से मनोरंजन सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए लगातार तीसरी बार पार्षद पद पर कब्जा जमाया. पिछली बार महिला आरक्षण के कारण उनकी पत्नी पूजा कुमारी चुनाव मैदान में उतरी थीं और जीत दर्ज की थी. इस बार चुनाव मैदान में उतरे मनोरंजन सिंह ने जीत दर्ज की. वहीं तीन बार पार्षद रह चुके निर्मल मुखर्जी को इस बार हार का सामना करना पड़ा. विकास रंजन ने उन्हें शिकस्त दी.
अरुणा ने दूसरी बार दर्ज की जीत
अरुणा कुमारी ने दूसरी बार जीत दर्ज कर अपनी सीट बरकरार रखी. हालांकि, वर्ष 2010 में उनके पति अशोक यादव ने इस वार्ड से जीत हासिल की थी. मीनाक्षी सिंह ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर अपना प्रभाव कायम रखा. इस वार्ड में पहले मीनाक्षी सिंह ने दर्ज की थी. दूसरी बार उनकी सास उषा सिंह जीत दर्ज की थी. कार्यकाल में ही उषा सिंह के निधन पर मिड टर्म में चुनाव हुआ था, जिसमें उनकी ननद सुमन सिंह ने जीत दर्ज की थी. इससे यह सीट लंबे समय से एक ही परिवार के कब्जे में रही. इधर, अंदिला कुमारी को मतदाताओं ने इस बार नकार दिया. पूर्व पार्षद प्रफुल्ल मंडल की पत्नी उर्मिला मंडल ने उन्हें हराया. वहीं वार्ड नंबर 52 से पूर्व पार्षद प्रियंका देवी को भी हार का सामना करना पड़ा. लक्ष्मी कुमारी ने उन्हें शिकस्त दी.
कड़ी सुरक्षा में मतगणना
धनबाद नगर निकाय चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पॉलिटेक्निक परिसर में जारी है. पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह की अव्यवस्था या हंगामे की आशंका को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं. पूरे परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं. एसएसपी प्रभात कुमार स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं. उनके नेतृत्व में सिटी एसपी सहित कई थाना प्रभारियों और बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की ड्यूटी लगाई गई है.
कई स्थानों पर की गई बैरिकेडिंग
भीड़ व समर्थकों को मतगणना स्थल से दूर रखने के लिए बेकारबांध स्थित चंद्रशेखर आजाद चौक पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है. वहीं, वीआइपी कॉलोनी मोड़ पर भी बैरिकेडिंग की गई है. दोनों स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी व जवानों की तैनाती की गई है. यहां आने-जाने वाले वाहनों और लोगों की सघन जांच की जा रही है. बिना पास के किसी को भी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है. इसके अलावा, कई थानों में अतिरिक्त पुलिस बल को रिजर्व रखा गया है. काउंटिंग स्थल के अंदर व बाहर दंडाधिकारी भी तैनात हैं.


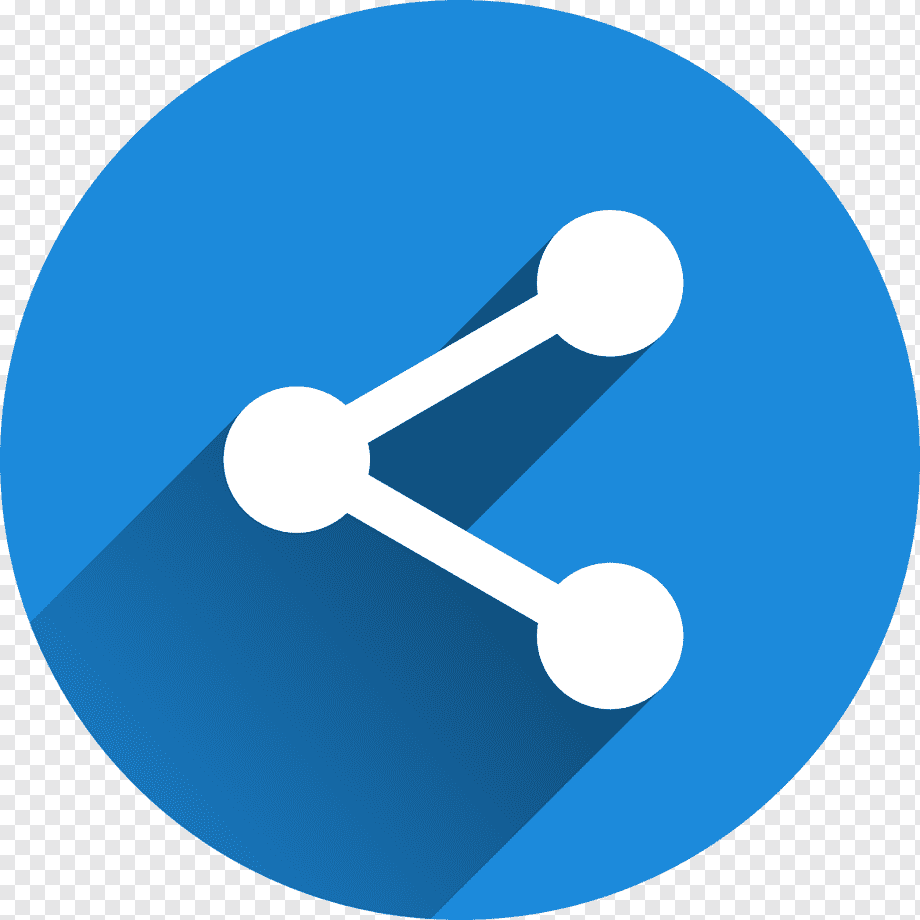





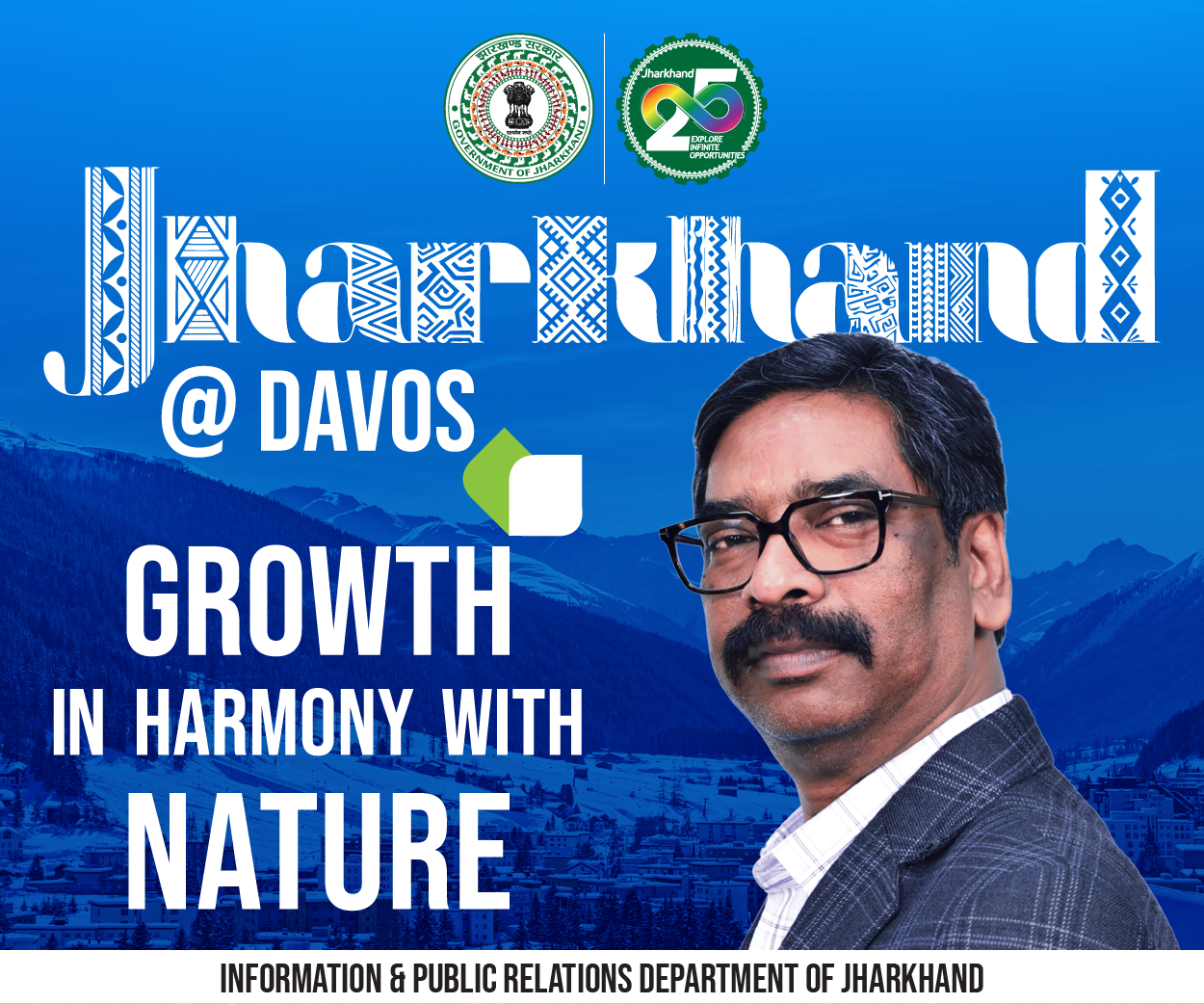


10 hours ago
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
1- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
1.5k